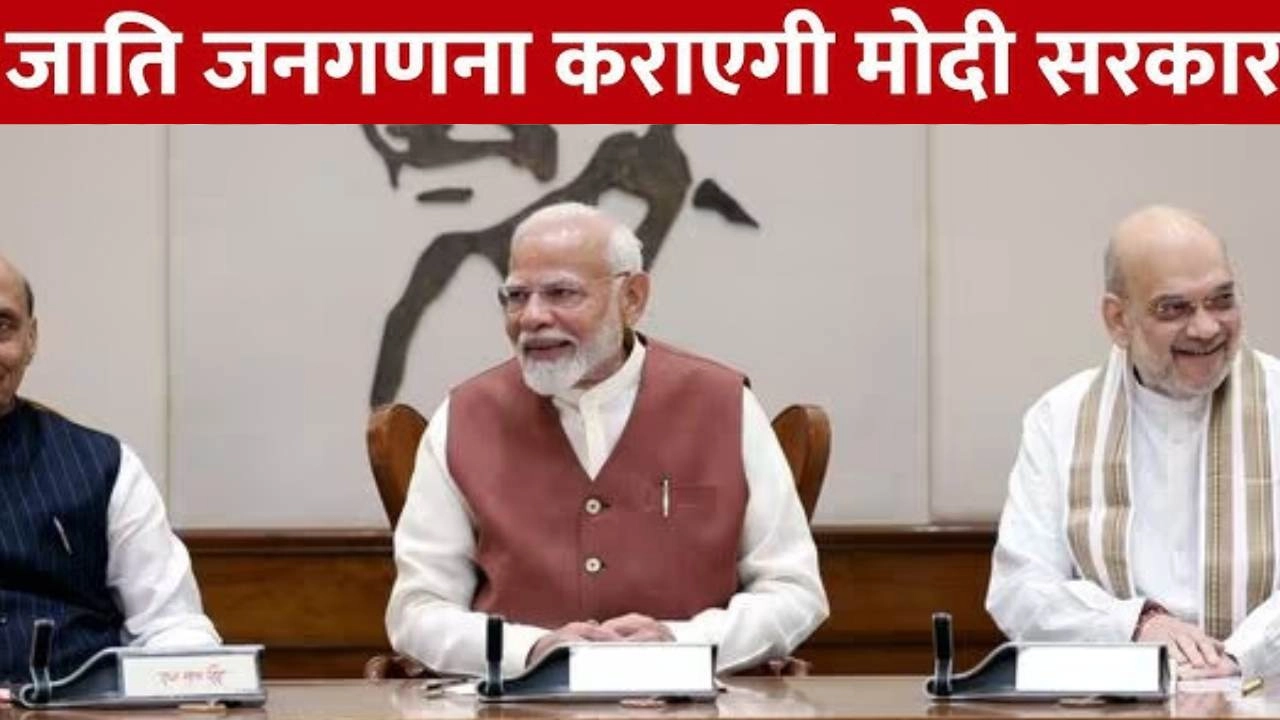
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना के दौरान जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। बीते वर्षों में कई विपक्षी पार्टियों ने इस मांग को लगातार उठाया और इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया है। जातीय जनगणना सिर्फ एक आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है।
क्या है जातीय जनगणना का मतलब?
जब किसी जनगणना में नागरिकों से उनकी जाति के बारे में पूछकर डेटा इकट्ठा किया जाता है तो उसे जातीय जनगणना कहा जाता है। यह प्रक्रिया बताती है कि कौन सी जाति किस इलाके में ज्यादा है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और शासन-प्रशासन में उनकी कितनी भागीदारी है।
भारत में जाति एक संवेदनशील और बहुस्तरीय विषय है जो न केवल सामाजिक संरचना बल्कि आरक्षण नीति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास योजनाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए ये आंकड़े सरकार को समाज के पिछड़े वर्गों तक योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।
फिलहाल किसको कितना मिलता है आरक्षण?
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 27%
अनुसूचित जाति (SC): 15%
अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%
जातीय जनगणना का इतिहास
भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी जिसमें जातियों की गिनती भी शामिल थी। 1931 तक हर जनगणना में जातियों के आंकड़े दर्ज किए जाते थे। उस समय भारत में 4,147 जातियां दर्ज की गई थीं।
आज की स्थिति यह है कि केवल महाराष्ट्र में ही जातियों की संख्या 4.10 लाख से ज्यादा हो चुकी है जबकि 1931 में यह आंकड़ा सिर्फ 494 था। देशभर में जातियों की संख्या बढ़कर 46 लाख तक पहुंच गई है।
आजादी के बाद क्यों बंद हुई जातीय जनगणना?
1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह तय किया कि अब सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) के आंकड़े ही इकट्ठा किए जाएंगे ताकि जातीय आधार पर समाज में और विभाजन न हो।
सरकार का मानना था कि सभी जातियों की गिनती करवाना सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद ओबीसी और अन्य जातियों के आंकड़े इकट्ठा नहीं किए गए जिससे उनकी सही स्थिति का आकलन कठिन हो गया।
2011 में फिर हुई थी जातीय जनगणना, लेकिन आंकड़े नहीं हुए सार्वजनिक
2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने करीब 4,500 करोड़ रुपये खर्च कर सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना करवाई थी। हालांकि इस जनगणना के जातीय आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए।
देश में ओबीसी की आबादी
सन् 1955 में: 32%
सन् 1990 में: 52%
सन् 1999 में: 36%
सन् 2004-05 में: 41%
सन् 2021-22 में: 46%
ये आंकड़े विभिन्न रिपोर्टों से लिए गए हैं जिनमें बताया गया है कि ये आंकड़े ओबीसी की जनसंख्या का एक अनुमान मात्र है इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।
इन राज्यों ने शुरू किया जातीय सर्वे
बिहार: 2023 में जातीय सर्वे कराया गया जिसमें पता चला कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों की संख्या राज्य की कुल आबादी का 63% से अधिक है।
कर्नाटक और तेलंगाना: इन राज्यों ने भी अपने स्तर पर जातीय सर्वेक्षण कराए हैं ताकि कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सके।
जातीय जनगणना के फायदे
1. ओबीसी और अन्य जातियों की सटीक जनसंख्या जानकर बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी।
2. हाशिए पर रह रहे समुदायों तक विकास योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाया जा सकता है।
3. इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाने में भी मदद मिल सकती है।
जातीय जनगणना का विरोध क्यों?
कुछ लोगों का मानना है कि जातीय जनगणना से समाज में जातिवाद और बढ़ेगा। यह तर्क दिया जाता है कि इससे सामाजिक एकता को नुकसान हो सकता है और समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इसके अलावा आलोचकों का यह भी कहना है कि सरकार के पास पहले से ही सामाजिक-आर्थिक डेटा मौजूद है जिसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सकता है।